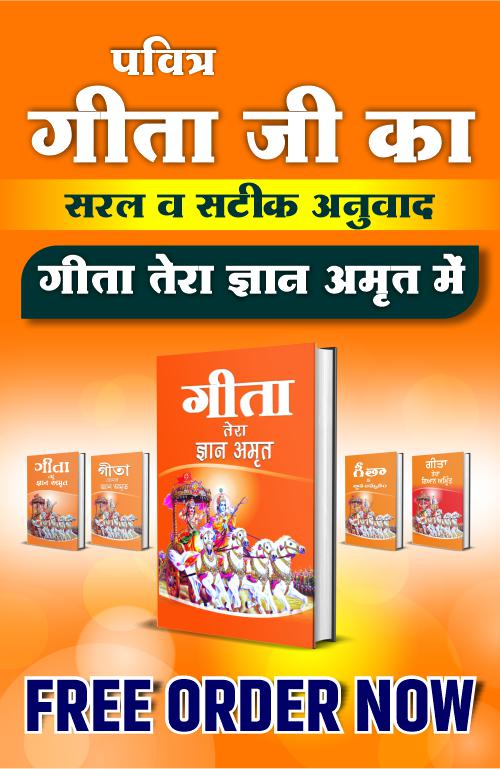अध्याय 6 श्लोक 1: जो साधक कर्मफलका आश्रय न लेकर शास्त्र विधि अनुसार करनेयोग्य भक्ति कर्म करता है वह सन्यासी अर्थात् शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों को त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थात् भक्त है और वासना रहित नहीं है तथा केवल एक स्थान पर बैठ कर विशेष आसन आदि लगा कर लोक दिखावा करके क्रियाओंका त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दम्भ करता है मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है वह न सन्यासी है, न ही कर्मयोगी अर्थात् भक्त है।
अध्याय 6 श्लोक 2: हे अर्जुन! जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उस भक्ति ज्ञान योग को जान क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता।
अध्याय 6 श्लोक 3: योग अर्थात् भक्ति में आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मननशील साधकके लिये शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही हेतु अर्थात् भक्ति का उद्देश्य कहा जाता है उस भक्ति में संलग्न साधकका जो सर्वसंकल्पोंका अभाव है वही वास्तव में भक्ति करने का कारण अर्थात् हेतु कहा जाता है।
अध्याय 6 श्लोक 4: जिस समयमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कर्मोंमें ही आसक्त होता है उस स्थितिमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न कहा जाता है।
अध्याय 6 श्लोक 5: पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है के तत्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा अपनी आत्माका उद्धार करे और अपनेको बर्बाद न करे क्योंकि शास्त्रा अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, इसलिए वह आत्म रूप परमात्मा वास्तव में आत्माका मित्र है और शास्त्रा विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीवात्मा वास्तव में स्वयं का शत्रु है।
अध्याय 6 श्लोक 6: जो आत्मा शास्त्रानुकूल साधना करता है उसका पूर्ण परमात्मा ही साथी है जिस कारण से वास्तव में शास्त्रा अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है जैसे बिजली का कनेक्शन लेने पर मानव शक्ति से न होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। ऐसे पूर्ण परमात्मा से जीवात्मा की विजय होती है अर्थात् सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है तथा परमगति को अर्थात् पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा मन व इन्द्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। परन्तु इसके विपरीत जो शास्त्रा अनुकूल साधना नहीं करते उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता, वह केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता रहता है इसलिए पूर्ण प्रभु के सहयोग रहित जीवात्मा स्वयं दुश्मन जैसा व्यवहार करता है वास्तव में वह साधक अपना ही शत्रु तुल्य है अर्थात् शास्त्रा विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात् मनमुखी पूजायें करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है न ही कार्य सिद्ध होता है, न परमगति ही प्राप्त होती है, प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24।
अध्याय 6 श्लोक 7: उपरोक्त श्लोक 6 में जिस विजयी आत्मा का विवरण है उसी से सम्बन्धित है कि वह परमात्मा के कृप्या पात्र विजयी आत्मा अर्थात् शास्त्रा अनुकूल साधना करने से प्रभु से सर्व सुख व कार्य सिद्धि प्राप्त हो रही है वह पूर्ण संतुष्ट साधक पूर्ण प्रभु के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित है अर्थात् उसको किसी अन्य से लाभ की चाह नहीं रहती। वह तो सर्दी व गर्मी अर्थात् सुख व दुःख में तथा मान व अपमान में भी प्रभु की इच्छा जान कर ही निश्चिंत रहता है।
अध्याय 6 श्लोक 8: जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञान अर्थात् तत्वज्ञान से तृप्त है जिसकी जीवात्मा की स्थिति विकाररहित है प्रभु के सहयोग से जिसकी इन्द्रियाँ भलीभाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान हैं वह शास्त्रा अनुकूल साधक युक्त अर्थात् भगवत्प्राप्त है यह अन्तिम ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है।
अध्याय 6 श्लोक 9: सुहृद्, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बन्धुगणोंमें धर्मात्माओंमें और पापियों में भी समान भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है।
अध्याय 6 श्लोक 10: मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला आशारहित और संग्रहरहित साधक अकेला ही एकान्त स्थानमें रहता है तथा स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगावे।
अध्याय 6 श्लोक 11: शुद्ध स्थान में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्रा बिछे हैं जो न बहुत ऊँचा है और न बहुत नीचा ऐसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके।
अध्याय 6 श्लोक 12: उस आसनपर बैठकर चित और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हुए मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये साधना का अभ्यास करे।
अध्याय 6 श्लोक 13: काया सिर और गर्दन को समान एवम् स्थिर धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभागपर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओंको न देखता हुआ।
अध्याय 6 श्लोक 14: ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित भयरहित तथा भलीभाँति शान्त अन्तःकरणवाला मनको रोककर लीन चितवाला मतावलम्बी मत् अनुसार अर्थात् जो काल विचार दे रहा है ऐसे करता हुआ साधना में संलग्न स्थित होवे।
अध्याय 6 श्लोक 15: इस प्रकार निरन्तर मेरे द्वारा उपरोक्त हठयोग बताया गया है उस के अनुसार मन को वश में करके स्वयं को परमात्मा के साधना में लगाता हुआ जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त होने वाले नियमित सिद्धांत के आधार से मेरे ही ऊपर आश्रित रहने वाला साधक अति शान्त अर्थात् समाप्त प्रायः शान्ति को प्राप्त होता है अर्थात् मेरे से मिलने वाली नाम मात्र मुक्ति को प्राप्त होता है। अपनी मुक्ति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं ही अति अश्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में अनिर्वणम् का अर्थात् न उकताए अर्थात् न मुर्झाए किया है इसलिए निर्वाणम् का अर्थ मुर्झायी हुई अर्थात् मरी हुई नाम मात्र की शान्ति हुई।
अध्याय 6 श्लोक 16: उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि वाली एकान्त में बैठ कर विशेष आसन आदि लगा कर साधना करना तो मेरे तक का लाभ प्राप्ति मात्र है, यह वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपने द्वारा दिए जाने वाले लाभ को अश्रेष्ठ बताया है। इसलिए हे अर्जुन इसके विपरीत उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकान्त स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात् व्रत रखने वाले की तथा न ही बहुत शयन करने वाले की तथा न ही हठ करके अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है अर्थात् उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि व्यर्थ है।
अध्याय 6 श्लोक 17: दुःखोंका नाश करनेवाला भक्ति तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका शास्त्र अनुसार कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागने वालेका ही सिद्ध होता है।
अध्याय 6 श्लोक 18: एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति में अत्यन्त नियमित किया हुआ चित जिस स्थितिमें परमात्मा में ही भलीभाँति स्थित हो जाता है उस कालमें सम्पूर्ण मनोकामनाओंसे मुक्त भक्तियुक्त अर्थात् भक्ति में संलग्न है ऐसा कहा जाता है।
अध्याय 6 श्लोक 19: जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान नहीं होता वैसी ही उपमा शास्त्रा अनुकूल साधक आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा अर्थात् पूर्ण ब्रह्म की साधना में लगे हुए प्रयत्न शील साधक के चितकी सुमरण स्थिति कही गयी है।
अध्याय 6 श्लोक 20: चित निरुद्ध योगके अभ्याससे जिस अवस्थामें ऊपर बताए मत - विचारों पर आधारित हो कर उपराम हो जाता है और जिस अवस्थामें शास्त्रा अनुकूल साधक जीवात्मा द्वारा आत्मा के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को सर्वत्र देखकर ही वास्तव में आत्मा से अभेद पूर्ण परमात्मा में संतुष्ट रहता है अर्थात् वह डगमग नहीं रहता।
अध्याय 6 श्लोक 21: इन्द्रियोंसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है। कभी न समाप्त होने वाला सुख अर्थात् पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और वास्तव में इस प्रकार स्थित यह योगी तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता।
अध्याय 6 श्लोक 22: केवल एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्रा अनुकूल साधना से एक ही प्रभु पर मन को रोकने वाले साधक जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और जिस कारण से सत्य भक्ति पर अडिग साधक बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता।
अध्याय 6 श्लोक 23: अज्ञान अंधकार से अज्ञात पूर्ण परमात्मा के वास्तविक भक्ति ज्ञान को जानना चाहिए। जो पापकर्मों के संयोग से उत्पन्न दुःख का अन्त अर्थात् छूटकारा करता है वह भक्ति न उकताये अर्थात् न मुर्झाए् हुए चितसे निश्चयपूर्वक करना कत्र्तव्य है अर्थात् करनी चाहिए।
अध्याय 6 श्लोक 24: संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको वास्तव में जड़ामूल से अर्थात् समूल त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके सभी ओरसे भलीभाँति रोककर।
अध्याय 6 श्लोक 25: धीरे-धीरे अभ्यास करता हुआ उपरोक्त दिए गए मत अर्थात् ज्ञान विचार द्वारा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको पूर्ण परमात्मा में टिका कर अर्थात् स्थित करके कुछ भी चिन्तन न करे।
अध्याय 6 श्लोक 26: यह स्थिर न रहनेवाला और चंचल मन जहाँ-जहाँ विचरता है उस उससे हटाकर शास्त्र अनुकूल साधक पूर्ण परमात्मा की कृप्या पात्र आत्मा अपने पूर्ण प्रभु के सहयोग से ही मनवश करे।
अध्याय 6 श्लोक 27: शास्त्र विधि त्यागकर साधना करना पाप है इसलिए इस पाप को निश्चय ही त्याग कर जिस शास्त्र अनुकूल साधक का मन भली प्रकार एक पूर्ण परमात्मा में शांत है जो पापसे रहित है, जो भौतिक सुख नहीं चाहता परमात्मा के हंस विधिवत् साधक को उत्तम आनन्द प्राप्त होता है अर्थात् पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है।
अध्याय 6 श्लोक 28: पापरहित साधक इस प्रकार निरन्तर साधना करता हुआ अपने समर्पण भाव से सुखपूर्वक पूर्ण परमात्मा के मिलन रूप कभी समाप्त न होने वाले आनन्दका अनुभव करता है अर्थात् पूर्ण मुक्त हो जाता है।
अध्याय 6 श्लोक 29: भक्तियुक्त आत्मावाला सबमें समभावसे देखनेवाला पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में है उसको सम्पूर्ण प्राणियों में स्थित और सम्पूर्ण प्राणियों को अपने समान अर्थात् जैसा दुःख व सुख अपने होता है इस दृष्टिकोण से देखता है।
अध्याय 6 श्लोक 30: जो सब जगह मुझे देखता है और सर्व को मुझमें देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता अर्थात् वह तो मेरे ही जाल में मेरी दृृष्टि है उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है।
अध्याय 6 श्लोक 31: जो एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित मुझे भजता है वह योगी सब प्रकारसे इस समय भी मुझमें ही बरतता है।
अध्याय 6 श्लोक 32: हे अर्जुन! जो योगी शास्त्रा अनुकूल साधना से आत्मा पूर्ण परमात्मा की कृृप्या पात्र हो जाती है उस पर प्रभु की विशेष कृृपा होने से वह स्वयं भी परमात्मा की उपमा जैसा हो जाता है, इसलिए आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को सब जगह तथा सर्व प्राणियों में सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है वह शास्त्रानुकूल आचरण वाला योगी श्रेष्ठ है।
अध्याय 6 श्लोक 33: हे मधुसूदन! जो यह योग आपने समभावसे कहा है मनके चंचल होनेसे मैं इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ।
अध्याय 6 श्लोक 34: क्योंकि हे श्रीकृृष्ण! यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाववाला बड़ा दृढ़ और बलवान् है। इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुको रोकनेकी भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ।
अध्याय 6 श्लोक 35: हे महाबाहो! निःसन्देह मन चंचल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है परंतु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह अभ्यास और वैराग्यसे वशमें होता है।
अध्याय 6 श्लोक 36: जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है अर्थात् जो संयमी नहीं ऐसे पुरुषद्वारा भक्ति दुष्प्राप्य है परन्तु शास्त्रा विधि अनुसार साधना करने वाले अर्थात् मनमानी पूजा न करके वशमें किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधनसे उसका प्राप्त होना सम्भव है यह मेरा मत अर्थात् विचार है।
अध्याय 6 श्लोक 37: हे श्रीकृृष्ण! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला है, किंतु जो संयमी नहीं है जिसका मन योगसे विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योगकी सिद्धिको अर्थात् न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है।
अध्याय 6 श्लोक 38: हे महाबाहो! क्या वह पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ मूर्ख शास्त्रा विधि त्याग कर साधना करने वाले साधक को प्रभु का आश्रय प्राप्त नहीं होता ऐसा आश्रयरहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? दुष्प्राय है अर्थात् भक्ति लाभ नहीं है। वह योग तो मनवश किए हुए को ही शक्य है। विचार करें फिर श्लोक 40 का यह अर्थ करना कि वह योग भ्रष्ट व्यक्ति न तो इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में, न्याय संगत नहीं है। क्योंकि अध्याय 6 श्लोक 42 से 44 में भी यही प्रमाण है कहा है योग भ्रष्ट व्यक्ति योग भ्रष्ट होने से पूर्व के भक्ति संस्कार से कुछ दिन स्वर्ग में जाता है फिर अच्छे कुल में जन्म प्राप्त करता है परन्तु पुनः वह मानव जन्म इस लोक में अत्यन्त दुर्लभ है। यदि मानव जन्म प्राप्त हो जाता है तो पूर्व के स्वभाववश मनमाना आचरण करके तत्वज्ञान का उल्लंघन कर जाता है। अर्थात् नष्ट हो जाता है। इसलिए श्लोक 40 का अनुवाद उपरोक्त सही है। अध्याय 6 श्लोक 45 में भी स्पष्ट है।
अध्याय 6 श्लोक 39: हे श्री कृष्ण! मेरे इस संशयको सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आपही योग्य हैं क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है।
अध्याय 6 श्लोक 40: हे पार्थ! वास्तव में पथ भ्रष्ट साधक न तो यहाँ का रहता है न वहाँ का रहता है। उसका विनाश ही जाना जाता है निसंदेह कोई भी व्यक्ति जो अन्तिम स्वांस तक मर्यादा से आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाला नहीं है अर्थात् जो योग भ्रष्ट हो जाता है हे प्रिय वह तो दुर्गति को चला जाता है अर्थात् प्राप्त होता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 40 में भी है।
अध्याय 6 श्लोक 41: योगभ्रष्ट पुरुष चैरासी लाख योनियों के कष्ट के बाद पुण्य कर्मों के आधार पर पुण्यवानोंके लोकोंको अर्थात् स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होकर उनमें वेद वाणी के आधार से नियत समय तक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले अच्छे विचारों वाले अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्तियों के घरमें जन्म लेता है, नीचे वाले श्लोक 43 में कहा है कि ऐसा जन्म दुर्लभ है।
अध्याय 6 श्लोक 42: अथवा ज्ञानवान् योगियोंके कुलमें जन्म लेता है। वास्तव में इस प्रकारका जो यह जन्म है सो संसारमें निःसन्देह अत्यन्त दुर्लभ है।
अध्याय 6 श्लोक 43: यदि वहाँ वह पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धिके संयोगको अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन! उसके पश्चात् फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके लिये प्रयत्न करता है।
अध्याय 6 श्लोक 44: वह पथभ्रष्ट साधक स्वभाव वश विवश हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही वास्तव में आकर्षित किया जाता है क्योंकि परमात्मा की भक्ति का जिज्ञासु भी परमात्मा की भक्ति विधि जो सद्ग्रन्थों में वर्णित है उस विधि अनुसार साधना न करके पूर्व के स्वभाव वश विचलित होकर उस वास्तविक नाम का जाप न करके प्रभु की वाणी रूपी आदेश का उल्लंघन कर जाता है। क्योंकि पूर्व स्वभाववश फिर विचलित हो जाता है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में जिज्ञासु को अच्छा नहीं कहा है केवल ज्ञानी भक्त जो एक परमात्मा की भक्ति करता है वह श्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 58 में भी प्रमाण है।
अध्याय 6 श्लोक 45: इसके विपरीत शास्त्रा अनुकुल साधक जिसे पूर्ण प्रभु का आश्रय प्राप्त है वह संयमी अर्थात् मन वश किया हुआ प्रयत्नशील सत्यभक्ति के प्रयत्न से अनेक जन्मों की भक्ति की कमाई से भक्त पाप रहित होकर तत्काल उसी जन्म में श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।
अध्याय 6 श्लोक 46: भगवान कह रहा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके साधना करने वाला नाम साधक मेरे द्वारा दिया अटकल लगाया साधना का मत अर्थात् पूजा विधि के ज्ञान अनुसार जो श्लोक 10 से 15 तक में हठ योग का विवरण दिया है उनमें जो हठ करके भक्ति कर्म से जो साधना करते हैं उन तपस्वियों से गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में वर्णित ज्ञानियों से तथा कर्म करने वाले से अर्थात् शास्त्राविरूद्ध साधना करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहे तत्वदर्शी संत की खोज करके उस से उपदेश प्राप्त करके शास्त्रा अनुकूल भक्त हो। गीता अध्याय 2 श्लोक 39 से 53 तक में कहा है कि हे अर्जुन! जिस समय तेरा मन भाँति-भाँति के ज्ञान वचनों से हट कर एक तत्वज्ञान पर स्थित हो जाएगा तब तो तू योग को प्राप्त होगा अर्थात् योगी बनेगा।
अध्याय 6 श्लोक 47: सर्व योगियों में भी जो श्रद्धावान साधक मेरे द्वारा दिए भक्ति मत अनुसार अन्तरात्मा से मुझको भजता है वह योगी मेरे मत अनुसार यथार्थ विधि से भक्ति में लीन है।